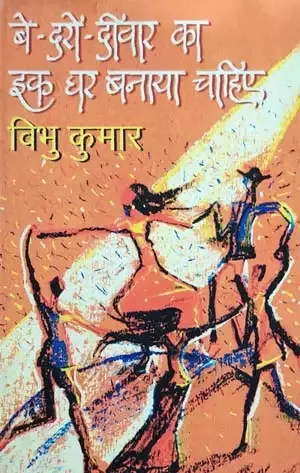|
नाटक-एकाँकी >> बे-दरो-दीवार का इक घर बनाया चाहिए बे-दरो-दीवार का इक घर बनाया चाहिएविभु कुमार
|
156 पाठक हैं |
||||||
आज के संदर्भ में और आने वाले कल के संदर्भ में यह नाटक महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगिक ठहरता है...
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
विभु कुमार अक्सर अपने नाटकों के माध्यम से हमारे समय के उन ज्वलंत और
मूलभूत सवालों को उठाने का यत्न करते हैं, जिनसे हमारे समय के अनेक
महत्त्वपूर्ण रचनाकार कतरा कर निकल जाते हैं। विभु कुमार हमारे समय में
ओझल उन जटिल विषयों को अपने अद्भुत नाटकीय कौशल से एक संपूर्ण नाटक में
बदल देते हैं। उनके नाटकों को पढ़ने का अर्थ है, हमारे समय और समाज की उन
अनेक विद्रूपताओं से गहरा साक्षात्कार, जिन्हें जाने बिना हम अपने समय और
समाज को ठीक-ठीक नहीं जान सकते।
विभु कुमार का यह नाटक- ‘बे-दरो-दीवार का इक घर बनाया चाहिए’ महाकवि ग़ालिब की आशा और आकांक्षा के अनुरूप एक ऐसे घर की कामना है, जहां न परस्पर अविश्वास हो, न तनाव, जहां परस्पर विश्वास और प्रेम की केवल छत भर हो। यह बात ग़ालिब के समय में जितनी सच थी, आज भी उतनी ही सच है।
यह नाटक घर को संकीर्ण अर्थ में ग्रहण न करते हुए संपूर्ण राष्ट्र को एक व्यापक अर्थ में प्रतिध्वनित करता है- जिसका एक वैश्विक संदर्भ भी है, एक ऐसा विश्व है जो न मज़हबी खांचों में बंटा हो, जहां धर्म की संकीर्णताएं मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवार बनकर खड़ी हों। यह नाटक मनुष्य को केवल एक मनुष्य के रूप में देखे और चीन्हे जाने की मांग करता है। इस तरह यह नाटक एक ऐसे सुंदर समाज की मांग करता है, जिसमें मज़हबी दरवाज़े और सांप्रदायिकता की दीवारें न हों-प्यार और परस्पर विश्वास के अलावा जहां कुछ भी और न हो।
इस अर्थ में यह नाटक आज के संदर्भ में और आने वाले कल के संदर्भ में भी एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगिक नाटक ठहरता है, कालजयी कृति होने की तमाम संभावनाओं को समाहित किए हुए।
विभु कुमार का यह नाटक- ‘बे-दरो-दीवार का इक घर बनाया चाहिए’ महाकवि ग़ालिब की आशा और आकांक्षा के अनुरूप एक ऐसे घर की कामना है, जहां न परस्पर अविश्वास हो, न तनाव, जहां परस्पर विश्वास और प्रेम की केवल छत भर हो। यह बात ग़ालिब के समय में जितनी सच थी, आज भी उतनी ही सच है।
यह नाटक घर को संकीर्ण अर्थ में ग्रहण न करते हुए संपूर्ण राष्ट्र को एक व्यापक अर्थ में प्रतिध्वनित करता है- जिसका एक वैश्विक संदर्भ भी है, एक ऐसा विश्व है जो न मज़हबी खांचों में बंटा हो, जहां धर्म की संकीर्णताएं मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवार बनकर खड़ी हों। यह नाटक मनुष्य को केवल एक मनुष्य के रूप में देखे और चीन्हे जाने की मांग करता है। इस तरह यह नाटक एक ऐसे सुंदर समाज की मांग करता है, जिसमें मज़हबी दरवाज़े और सांप्रदायिकता की दीवारें न हों-प्यार और परस्पर विश्वास के अलावा जहां कुछ भी और न हो।
इस अर्थ में यह नाटक आज के संदर्भ में और आने वाले कल के संदर्भ में भी एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगिक नाटक ठहरता है, कालजयी कृति होने की तमाम संभावनाओं को समाहित किए हुए।
रमेश अनुपम
कवि एवं समीक्षक
कवि एवं समीक्षक
दो रंग-निर्देशकों के मंचन पूर्व वक्तव्य
मूलत: विभु कुमार की रंग-यात्रा, एक नाटककार के रूप में, नुक्कड़ से
प्रारंभ हुई थी। वस्तुत: वे स्वयं एक सशक्त अभिनेता भी हैं। रंगमंचीय
नाटकों में यद्यपि उन्होंने अभिनय नहीं किया परंतु नुक्कड़ नाटक में जो
व्यक्ति अभिनय से पात्र को सजीव करता है वह एक सशक्त अभिनेता होता है।
एक साहित्यकार और हिन्दी के प्राध्यापक होने के कारण सटीक शब्द-संयोजन के द्वारा भावनाओं और विचारों का सीधा संप्रेषण करने में भी वे समर्थ हैं। इसी कारण विभु कुमार के नाटक दर्शकों के दिल और दिमाग़ से सीधा संवाद स्थापित कर लेते हैं।
मुन्नीबाई जैसे सशक्त नाटक के सर्जक विभु कुमार ने उतने ही संभवत: अधिक गहरी अनुभूति से इस नाटक की रचना की है। मुन्नीबाई की रचना शायद उन्होंने तटस्थ भाव से की होगी परंतु इस नाटक में विभु कुमार एक क़दम आगे जा कर पात्रों की त्रासदी को मानो स्वयं भोग रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। प्रसंगों की नाट्यमयता और भावनाओं का सहज प्रकटीकरण इस नाटक की विशेषता है।
अत्यंत सहज रूप में, मिस्त्री और रेज़ा के घर बनाने की प्रक्रिया को आधार बना कर, परिवार और देश के निर्माण के तथ्यों को यथार्थ के धरातल पर ला खड़ा किया है। धर्म या मज़हब की विवेकशून्य दीवारें हमारे परिवार को सुरक्षित छत प्रदान करने में अक्षम क्यों हैं ? इस प्रश्न का उत्तर विभु कुमार ने इस नाटक में तलाशने का यत्न किया है।
‘पुरुष’ तथा ‘स्त्री’ हमारे समाज में कहीं भी हो सकते हैं (शायद इसीलिए इन पात्रों को कोई नाम नहीं दिया गया)। इन दोनों पात्रों की रचना में, ‘नर और मादा’ के नैसर्गिक संबंधों को, अत्यंत संयम और सौंदर्यबोध के साथ दर्शाया है। वैसे ही पुरुषोचित ‘अहं’ और स्त्रियोचित ‘हठधर्मिता’-दोनों पात्रों की आत्मा है। नाटक में कहीं भी उन्हें काल्पनिक आदर्श का जामा नहीं पहनाया गया है। प्रत्येक प्रसंग में उनके उद्गार और व्यवहार एकदम सहज और सही प्रतीत होते हैं। इन्हीं कारणों से यह नाटक आम दर्शकों से सीधे जुड़ने में समर्थ प्रतीत होता है।
यही बात नाटक के पात्र लड़का-1 और लड़का-2 के साथ भी लागू होती है। ये दोनों नयी पीढ़ी और नयी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। नयी पीढ़ी बदलते सामाजिक परिवेश से प्रभावित है, जबकि पुरानी पीढ़ी अपने पुराने परिवेश के संस्कारों से प्रभावित है जो बदलाव को सहज स्वीकारने में न केवल कठिनाई महसूस करती है वरन् कुछ हद तक अपने दकियानूसी, कालतिरोहित विचारों की लाश को ढोते हुए प्रतीत होती है। जो संघर्ष को जन्म देती है। जिस घटना को पुरानी पीढ़ी ‘क्रान्तिकारी’ मान कर एक अंत के साथ जीना चाहती है, उसे नयी पीढ़ी एक अत्यंत सामान्य घटना मान कर चलती है। यहाँ पर दो पीढ़ियों के बीच सोच की खांई उत्पन्न होती है जो संघर्ष का कारण बन सकती है। नाटक में ‘जैनरेशन गैप’ का बड़ा सहज स्वरूप दिखाई देता है।
संपूर्ण नाटक में विचार और भावना के दो धरातलों पर संघर्ष होता दिखाई देता है। नाटककार विभु कुमार ने एक ओर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण, मज़हब की वैचारिक पृष्ठभूमि पर मां-बेटी, प्रेमी-प्रेमिका, सास-बहू, बाप-बेटा, स्त्री-पुरुष के भावावत्मक संबंधों में छिपे संघर्ष को उजागर किया है।
मंचन की दृष्टि से सभी प्रसंग और पात्र सहज और उचित व्यवहार करते प्रतीत होते हैं। नाटककार चूंकि अनेक नाट्यमंचनों से जुड़ा रहा है, अपनी रचना में जगह-जगह टिप्पणियां देता है मानो वह निर्दशक को निर्देशित कर रहा हो। निर्देशक का दायित्व उन टिप्पणियों जैसा निर्देशन करने मात्र से समाप्त नहीं हो जाएगा (वरना फिर निर्देशक की ज़रूरत ही क्या रहेगी !) वरना प्रस्तुति सपाट बन जाएगी।
इस नाट्यरचना में ‘मेक एंड ब्रेक’ शैली दिखाई पड़ती है। एक दृश्यबंध का वांछित प्रभाव उत्पन्न करना और दूसरे दृश्यबंध के पूर्व उसे तोड़ देना ताकि दूसरे का प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। ‘कटिन्यूटी’ (सततता) केवल ‘अंडरकरंट’ (भीतर से प्रवाहित) होती दिखाई देती है जो दर्शक पूरे मंचन में महसूस करे, यह ध्यान व विशेष रूप से रखना होगा।
मंच पर एक साथ दो घटनाएं भी घटती हैं-इनमें अंत:संबंध या कोरिलेश—प्रकाश, संगीत और अभिनय के माध्यम से स्थापित करना और दोनों में संतुलन बनाये रखना चुनौतीपूर्ण होगा।
अनेक प्रसंगों में अति भावुकता ‘मेलोड्रामा’ संभव है पर उसे टालने की कोशिश में यंत्रवत् अभिनय नाटक को प्रभावहीन भी कर सकता है, अत: इसका संतुलन बनाये रखना निर्देशक के साथ अभिनेताओं की बड़ी ज़िम्मेदारी होगी।
मंचसज्जा-आर्थिक संसाधन और अन्य साधनों की सुलभता तथा नेपथ्य रचनाकार की क्षमता पर निर्भर है। चाहे मंचन पारंपरिक शैली से हो चाहे ‘नो सेट थियरी’ के आधार पर, वस्तुत: वह रंगमंडली की क्षमता पर निर्भर होगा।
संपूर्ण रंगमंच को दो धरातलों में बांट कर भी दृश्यबंधों का संयोजन किया जा सकता है।
वर्तमान और अतीत के दो धरातल हो सकते हैं। नाटककार ने जगह जगह व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया है। इसे दोनों धरातलों का सम्मिलित प्रयोग कर दर्शाने से एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जहाँ तक प्रकाश व्यवस्था का प्रश्न है, स्पेशल और जनरल लाइटिंग से प्रस्तुति सुंदर बन सकती है। जहां पर नाटककार कुछ प्रश्न उपस्थित कर उनका उत्तर खोजने का यत्न करता है, वहां पर स्पॉटलाइट के प्रयोग से प्रभाव को गहरा किया जा सकता है।
संगीत का विचार करते समय फिल्मी गीतों या धुनों का प्रयोग मेरे विचार से दर्शकों को रंगमंचीय घटनाक्रम से बाहर निकाल देता है। इसलिए विभिन्न वाद्यों के प्रयोग से अलग-अलग समय और स्थिति की पृष्ठभूमि बन सकती है। वेशभूषा के संदर्भ में ये पात्र-स्त्री और पुरुष, मिस्त्री और रेज़ा-परिवार का मित्र, आर्थिक विपन्नता या पुरानी पीढ़ी के द्योतक हैं। अतः सामान्य वेश-भूषा उचित होगी। जबकि लड़का -1 और 2 नयी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जींस और चटख रंगों की टी-शर्ट्स उपयुक्त होंगे। दोनों पीढ़ियों के अंतर को भी अधिक गहराई से उजागर कर सकेंगे।
नाटक का ‘पुरुष’ जो मुख्य पात्र है, शायद अपराधबोध से भी ग्रसित दिखाई देता है और शायद यही कारण है कि ‘स्त्री’ पात्र को अंत में ‘गंगा’ और ‘आबेहयात’ के संबोधन से सम्मानित कर उस अपराधबोध पर परदा डालने की कोशिश की गयी है। यहां नाटक कुछ कमज़ोर प्रतीत होता है, संतुलन खोता दिखाई देता है। सामान्य तौर पर निर्देशक नाट्यसंहिता में संवादों में कोई हेर-फेर नहीं करता है। परंतु हो सकता है, इस नाटक के मंचन में कोई निर्देशक इसकी स्वतंत्रता ले, कहीं कांट-छांट कतरे या कुछ स्वरचित संवाद भी डाल दे। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।
नाटककार ने संपूर्ण नाटक में कहीं भी ‘इंटिग्रेशन’ जैसी थोथी बातों को न तो आदर्श बनाया है और न उसे प्रोजेक्ट किया है। मात्र जीवन के एक वास्तविकता से वह हमारा परिचय कराता है, और निर्देशक को भी बस उतना ही करना है-केवल सशक्तता से, सुव्यवस्थित रूप में, सौंदर्यबोध के साथ एक कलात्मक रूप में....बाक़ी सब दर्शकों को सोचना है।
एक साहित्यकार और हिन्दी के प्राध्यापक होने के कारण सटीक शब्द-संयोजन के द्वारा भावनाओं और विचारों का सीधा संप्रेषण करने में भी वे समर्थ हैं। इसी कारण विभु कुमार के नाटक दर्शकों के दिल और दिमाग़ से सीधा संवाद स्थापित कर लेते हैं।
मुन्नीबाई जैसे सशक्त नाटक के सर्जक विभु कुमार ने उतने ही संभवत: अधिक गहरी अनुभूति से इस नाटक की रचना की है। मुन्नीबाई की रचना शायद उन्होंने तटस्थ भाव से की होगी परंतु इस नाटक में विभु कुमार एक क़दम आगे जा कर पात्रों की त्रासदी को मानो स्वयं भोग रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। प्रसंगों की नाट्यमयता और भावनाओं का सहज प्रकटीकरण इस नाटक की विशेषता है।
अत्यंत सहज रूप में, मिस्त्री और रेज़ा के घर बनाने की प्रक्रिया को आधार बना कर, परिवार और देश के निर्माण के तथ्यों को यथार्थ के धरातल पर ला खड़ा किया है। धर्म या मज़हब की विवेकशून्य दीवारें हमारे परिवार को सुरक्षित छत प्रदान करने में अक्षम क्यों हैं ? इस प्रश्न का उत्तर विभु कुमार ने इस नाटक में तलाशने का यत्न किया है।
‘पुरुष’ तथा ‘स्त्री’ हमारे समाज में कहीं भी हो सकते हैं (शायद इसीलिए इन पात्रों को कोई नाम नहीं दिया गया)। इन दोनों पात्रों की रचना में, ‘नर और मादा’ के नैसर्गिक संबंधों को, अत्यंत संयम और सौंदर्यबोध के साथ दर्शाया है। वैसे ही पुरुषोचित ‘अहं’ और स्त्रियोचित ‘हठधर्मिता’-दोनों पात्रों की आत्मा है। नाटक में कहीं भी उन्हें काल्पनिक आदर्श का जामा नहीं पहनाया गया है। प्रत्येक प्रसंग में उनके उद्गार और व्यवहार एकदम सहज और सही प्रतीत होते हैं। इन्हीं कारणों से यह नाटक आम दर्शकों से सीधे जुड़ने में समर्थ प्रतीत होता है।
यही बात नाटक के पात्र लड़का-1 और लड़का-2 के साथ भी लागू होती है। ये दोनों नयी पीढ़ी और नयी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। नयी पीढ़ी बदलते सामाजिक परिवेश से प्रभावित है, जबकि पुरानी पीढ़ी अपने पुराने परिवेश के संस्कारों से प्रभावित है जो बदलाव को सहज स्वीकारने में न केवल कठिनाई महसूस करती है वरन् कुछ हद तक अपने दकियानूसी, कालतिरोहित विचारों की लाश को ढोते हुए प्रतीत होती है। जो संघर्ष को जन्म देती है। जिस घटना को पुरानी पीढ़ी ‘क्रान्तिकारी’ मान कर एक अंत के साथ जीना चाहती है, उसे नयी पीढ़ी एक अत्यंत सामान्य घटना मान कर चलती है। यहाँ पर दो पीढ़ियों के बीच सोच की खांई उत्पन्न होती है जो संघर्ष का कारण बन सकती है। नाटक में ‘जैनरेशन गैप’ का बड़ा सहज स्वरूप दिखाई देता है।
संपूर्ण नाटक में विचार और भावना के दो धरातलों पर संघर्ष होता दिखाई देता है। नाटककार विभु कुमार ने एक ओर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण, मज़हब की वैचारिक पृष्ठभूमि पर मां-बेटी, प्रेमी-प्रेमिका, सास-बहू, बाप-बेटा, स्त्री-पुरुष के भावावत्मक संबंधों में छिपे संघर्ष को उजागर किया है।
मंचन की दृष्टि से सभी प्रसंग और पात्र सहज और उचित व्यवहार करते प्रतीत होते हैं। नाटककार चूंकि अनेक नाट्यमंचनों से जुड़ा रहा है, अपनी रचना में जगह-जगह टिप्पणियां देता है मानो वह निर्दशक को निर्देशित कर रहा हो। निर्देशक का दायित्व उन टिप्पणियों जैसा निर्देशन करने मात्र से समाप्त नहीं हो जाएगा (वरना फिर निर्देशक की ज़रूरत ही क्या रहेगी !) वरना प्रस्तुति सपाट बन जाएगी।
इस नाट्यरचना में ‘मेक एंड ब्रेक’ शैली दिखाई पड़ती है। एक दृश्यबंध का वांछित प्रभाव उत्पन्न करना और दूसरे दृश्यबंध के पूर्व उसे तोड़ देना ताकि दूसरे का प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। ‘कटिन्यूटी’ (सततता) केवल ‘अंडरकरंट’ (भीतर से प्रवाहित) होती दिखाई देती है जो दर्शक पूरे मंचन में महसूस करे, यह ध्यान व विशेष रूप से रखना होगा।
मंच पर एक साथ दो घटनाएं भी घटती हैं-इनमें अंत:संबंध या कोरिलेश—प्रकाश, संगीत और अभिनय के माध्यम से स्थापित करना और दोनों में संतुलन बनाये रखना चुनौतीपूर्ण होगा।
अनेक प्रसंगों में अति भावुकता ‘मेलोड्रामा’ संभव है पर उसे टालने की कोशिश में यंत्रवत् अभिनय नाटक को प्रभावहीन भी कर सकता है, अत: इसका संतुलन बनाये रखना निर्देशक के साथ अभिनेताओं की बड़ी ज़िम्मेदारी होगी।
मंचसज्जा-आर्थिक संसाधन और अन्य साधनों की सुलभता तथा नेपथ्य रचनाकार की क्षमता पर निर्भर है। चाहे मंचन पारंपरिक शैली से हो चाहे ‘नो सेट थियरी’ के आधार पर, वस्तुत: वह रंगमंडली की क्षमता पर निर्भर होगा।
संपूर्ण रंगमंच को दो धरातलों में बांट कर भी दृश्यबंधों का संयोजन किया जा सकता है।
वर्तमान और अतीत के दो धरातल हो सकते हैं। नाटककार ने जगह जगह व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया है। इसे दोनों धरातलों का सम्मिलित प्रयोग कर दर्शाने से एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जहाँ तक प्रकाश व्यवस्था का प्रश्न है, स्पेशल और जनरल लाइटिंग से प्रस्तुति सुंदर बन सकती है। जहां पर नाटककार कुछ प्रश्न उपस्थित कर उनका उत्तर खोजने का यत्न करता है, वहां पर स्पॉटलाइट के प्रयोग से प्रभाव को गहरा किया जा सकता है।
संगीत का विचार करते समय फिल्मी गीतों या धुनों का प्रयोग मेरे विचार से दर्शकों को रंगमंचीय घटनाक्रम से बाहर निकाल देता है। इसलिए विभिन्न वाद्यों के प्रयोग से अलग-अलग समय और स्थिति की पृष्ठभूमि बन सकती है। वेशभूषा के संदर्भ में ये पात्र-स्त्री और पुरुष, मिस्त्री और रेज़ा-परिवार का मित्र, आर्थिक विपन्नता या पुरानी पीढ़ी के द्योतक हैं। अतः सामान्य वेश-भूषा उचित होगी। जबकि लड़का -1 और 2 नयी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जींस और चटख रंगों की टी-शर्ट्स उपयुक्त होंगे। दोनों पीढ़ियों के अंतर को भी अधिक गहराई से उजागर कर सकेंगे।
नाटक का ‘पुरुष’ जो मुख्य पात्र है, शायद अपराधबोध से भी ग्रसित दिखाई देता है और शायद यही कारण है कि ‘स्त्री’ पात्र को अंत में ‘गंगा’ और ‘आबेहयात’ के संबोधन से सम्मानित कर उस अपराधबोध पर परदा डालने की कोशिश की गयी है। यहां नाटक कुछ कमज़ोर प्रतीत होता है, संतुलन खोता दिखाई देता है। सामान्य तौर पर निर्देशक नाट्यसंहिता में संवादों में कोई हेर-फेर नहीं करता है। परंतु हो सकता है, इस नाटक के मंचन में कोई निर्देशक इसकी स्वतंत्रता ले, कहीं कांट-छांट कतरे या कुछ स्वरचित संवाद भी डाल दे। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।
नाटककार ने संपूर्ण नाटक में कहीं भी ‘इंटिग्रेशन’ जैसी थोथी बातों को न तो आदर्श बनाया है और न उसे प्रोजेक्ट किया है। मात्र जीवन के एक वास्तविकता से वह हमारा परिचय कराता है, और निर्देशक को भी बस उतना ही करना है-केवल सशक्तता से, सुव्यवस्थित रूप में, सौंदर्यबोध के साथ एक कलात्मक रूप में....बाक़ी सब दर्शकों को सोचना है।
निर्देशक
-प्रो. महाराष्ट्र नाट्य मंडल रायपुर (छत्तीसगढ़)
-प्रो. महाराष्ट्र नाट्य मंडल रायपुर (छत्तीसगढ़)
अनिल कालले
‘रंगकर्म’ मुझ जैसे के लिए मानसिक भूख मिटाने का
प्रिय व्यंजन
है। इसी तरह ‘नाटक’ देखना भी बहुतों के लिए बौद्धिक
मनोरंजन
करने का महत्त्वपूर्ण घटक हो सकता है।
आज के प्रेक्षकों के सामने मनोरंजन और बौद्धिक भूख मिटाने के लिए नाटक के अतिरिक्त कई साधन विलुपता से उपलब्ध हैं। यही कारण है कि कुछ अपवादात्मक नाटकों को छोड़ कर साधारणतया हिन्दी नाटकों को प्रेक्षकों की कमी हमेशा से खलती रही है। ‘नाटक’ देखने कितने प्रेक्षक आते हैं, इस बात को मैं महत्त्वपूर्ण नहीं मानता, बल्कि नाट्यसंहिता और उसके प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रेक्षकों का मत क्या है, इसे मैं ज्यादा जरूरी मानता हूँ। नाटक में ऐसा कौन सा विचार है या ऐसा कौन-सा पुराना विचार है जो आज भी उतना प्रासंगिक और ज्वलंत और नाटककार ने उसे कितनी ईमानदारी, हिम्मत और पूरे आशय के साथ लिखा है, इस बात पर उस नाटक का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। बदलते परिवेश के अनुरूप बदलती संवेदनाओं को साथ लेकर चलने वाला नाटक आज की ज़रूरत है। विभु कुमार का नाटक मेरी इन्हीं आशाओं, आकांक्षाओं पर जब खरा उतरने लगता है तो एक ही सांस में नाटक को पूरा पढ़ने के लिए मैं विवश हो जाता हूं।
रेती-सीमेंट, तसले-फावड़े की बेसुरी आवाज़ों के बीच जब अचानक विभु कुमार सांप्रदायिकता की छत, प्यार और आस्था का छप्पर, घर और मकान का फ़र्क़ समझाने मिस्त्री, रेज़ा को लाते हैं तो ख़याल आता है कि नाटक तो शुरू हो चुका है।
विभु कुमार ने अपना नायक चुना है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वप्नद्रष्टा है। तरल भावाभिव्यक्ति उसका मूल स्वभाव है जो किसी हद तक ठेठ हृदय तक जा कर भिड़ जाता है। फिर भी वह अपने अंदर के पुरातन पुरुष के उस गुण (या अवगुण) को मन के अंदर कहीं न कहीं अवश्य छुपाये बैठा है, उसी तरह जैसे जंगली जानवर किसी शिकार को नजदीक भांपकर घात लगाए बैठता है। यही विरोधाभास नायक को नाटक में बहुत जल्दी स्थापित कर देता है।
विभु कुमार का नायक ज़्यादातर शांत भाव से शरीफ़ाना अंदाज में बात करता है, लेकिन जब जब वह स्वगत भाष्य करता है, (होश में या मदहोशी में) तो वह जीवनशैली, जिंदगी जीने के अपने तरीक़े, धर्म नैतिकता के संबंध में अपने विचार बहुत सीधे और सपाट तरीक़े से सुनता है। उसकी सारी भावाभिव्यक्ति एक प्रगट-भाषण (Loud thinking) के रूप में विधानात्मक पद्धति से विभु कुमार अपनी विशेष शैली के द्वारा प्रस्तुत करते हैं।
इसके विपरीत नाटक की नायिका स्पष्टवादी, ज़िन्दगी को एक संघर्ष मान कर जीने वाली अपने विचारों पर चाहे वह कितनी ही Rigid क्यों न हो, अंत तक अड़े रहने वाली लेकिन साहसी महिला है जो समाज और धर्म को दरकिनार कर अपने प्रेमी से विवाह कर लेती है, लेकिन प्रेमी-प्रेमिका को परस्पर विश्वास का अंकुर पति-पत्नी बन जाने पर एक ‘वटवृक्ष’ की तरह उन्नत कराने में असहाय सिद्ध होती है और यहीं पर नाटक का आशय और मूल स्वभाव विभु कुमार स्पष्ट करते हैं।
नाटक में बोली जाने वाली भाषा चाहे वह ठेठ छत्तीसगढ़ी हो या उपनगरीय (यहां मेरा आशय ‘हिंग्लिश’ अर्थात् इंगलिश मिश्रित हिन्दी से है), संवाद ‘बोल्ड’ और प्रभावी हैं। विभु कुमार के नाटकों का शक्तिस्थान प्रभाव व स्फूर्त संवाद हैं।
उदाहरण: ‘आजादी के इतने वर्षों बाद भी यह देश एक छत के नीचे नहीं आ पाया है। जानते हो मिस्त्री, क्यों ? क्योंकि पचास वर्ष बाद भी ये राजनेता देश की छत तक नहीं ढाल पाये हैं।’
‘मकान में जब दो प्यार भरे दिल रहते हैं तब वह घर बनता है। ‘या’ सपने में अचानक धर्म कहां आ गया ? क्या सपनों का भी अलग अलग धर्म होता है ? या सपने भी हिंदू या मुसलमान होते हैं ?’
अपने अनूठे दृष्टिकोण और आक्रामक विचारों के बावजूद विभु कुमार मंचन की दृष्टि से निर्देशक को मेहनत-मशक्कत करवाने में कसर नहीं छोड़ते। अपने तेज़-तर्रार संवादों और शाब्दिक मायाजाल बुनने में वे पूरे खरे उतरे हैं। लेकिन नाट्यमंचन करने में सहायक ‘प्रसंग निर्मित’ में निर्देशक की मानो परीक्षा ले ली है। पहले अंक की समाप्ति तक पता चल जाता है
कि नाटक अपनी यही निर्बाध गति बनाये रखेगा और निर्देशक को अपनी क्रियाशीलता (Creativity) उसी गति से लगातार बनाये रखनी होगी व प्रसंगों को यथोचित (Directorial Touch) देते रहना होगा, वरना किस क्षण नाटक अचानक मोड़ ले कर प्रचार-नाट्य (Propaganda-play) की ओर झुकता जाएगा, इस बात पर अंकुश लगाना कठिन कार्य हो जाएगा।
यह बात कहकर मैं विभु कुमार के इस नाटक पर प्रचार-नाट्य का आरोप क़तई नहीं लगा रहा हूं। क्योंकि प्रचार-नाट्य किसी ख़ास विषय का तात्कालिक मुद्दों पर अपनी बात बहुत ही बोझिलाना अंदाज में प्रेक्षकों पर उंडेलते रहते हैं जैसे, स्त्रियों का शोषण, अंधविश्वास, पानी की समस्या या पर्यावरण आदि। इन नाटकों में विचारों को प्राधान्य दिया जाता है, लेकिन नाट्यमयता नदारद हो जाती है। ऐसे नाटक तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक विषय ताज़े हों। समस्याओं का समाधान होने पर नाटक स्वत: ही काल की गोद में चले जाते हैं।
विभु कुमार ने इस नाटक में भी कुछ समस्याओं को छुआ है, लेकिन समस्याओं का समाधान खोजने में उन्होंने प्रचार-तंत्र का सड़ा-गला रूप त्याग कर नये समाज के प्रतिरूप नौजवान पीढ़ी को अपने ताज़े रूप में प्रस्तुत कर इस दिशा में अलग रास्ता चुना है।
इस नाटक का नौजवान Charity begins at home के सिद्धान्त के अनुरूप वैचारिक परिवर्तन लाने गली-मुहल्ले या समाज से नहीं, बल्कि सीधे अपने घर से शुरूआत करने का बीड़ा उठाता है। इसी Positive note पर नाटक की इतिश्री होती है।
आज के प्रेक्षकों के सामने मनोरंजन और बौद्धिक भूख मिटाने के लिए नाटक के अतिरिक्त कई साधन विलुपता से उपलब्ध हैं। यही कारण है कि कुछ अपवादात्मक नाटकों को छोड़ कर साधारणतया हिन्दी नाटकों को प्रेक्षकों की कमी हमेशा से खलती रही है। ‘नाटक’ देखने कितने प्रेक्षक आते हैं, इस बात को मैं महत्त्वपूर्ण नहीं मानता, बल्कि नाट्यसंहिता और उसके प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रेक्षकों का मत क्या है, इसे मैं ज्यादा जरूरी मानता हूँ। नाटक में ऐसा कौन सा विचार है या ऐसा कौन-सा पुराना विचार है जो आज भी उतना प्रासंगिक और ज्वलंत और नाटककार ने उसे कितनी ईमानदारी, हिम्मत और पूरे आशय के साथ लिखा है, इस बात पर उस नाटक का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। बदलते परिवेश के अनुरूप बदलती संवेदनाओं को साथ लेकर चलने वाला नाटक आज की ज़रूरत है। विभु कुमार का नाटक मेरी इन्हीं आशाओं, आकांक्षाओं पर जब खरा उतरने लगता है तो एक ही सांस में नाटक को पूरा पढ़ने के लिए मैं विवश हो जाता हूं।
रेती-सीमेंट, तसले-फावड़े की बेसुरी आवाज़ों के बीच जब अचानक विभु कुमार सांप्रदायिकता की छत, प्यार और आस्था का छप्पर, घर और मकान का फ़र्क़ समझाने मिस्त्री, रेज़ा को लाते हैं तो ख़याल आता है कि नाटक तो शुरू हो चुका है।
विभु कुमार ने अपना नायक चुना है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वप्नद्रष्टा है। तरल भावाभिव्यक्ति उसका मूल स्वभाव है जो किसी हद तक ठेठ हृदय तक जा कर भिड़ जाता है। फिर भी वह अपने अंदर के पुरातन पुरुष के उस गुण (या अवगुण) को मन के अंदर कहीं न कहीं अवश्य छुपाये बैठा है, उसी तरह जैसे जंगली जानवर किसी शिकार को नजदीक भांपकर घात लगाए बैठता है। यही विरोधाभास नायक को नाटक में बहुत जल्दी स्थापित कर देता है।
विभु कुमार का नायक ज़्यादातर शांत भाव से शरीफ़ाना अंदाज में बात करता है, लेकिन जब जब वह स्वगत भाष्य करता है, (होश में या मदहोशी में) तो वह जीवनशैली, जिंदगी जीने के अपने तरीक़े, धर्म नैतिकता के संबंध में अपने विचार बहुत सीधे और सपाट तरीक़े से सुनता है। उसकी सारी भावाभिव्यक्ति एक प्रगट-भाषण (Loud thinking) के रूप में विधानात्मक पद्धति से विभु कुमार अपनी विशेष शैली के द्वारा प्रस्तुत करते हैं।
इसके विपरीत नाटक की नायिका स्पष्टवादी, ज़िन्दगी को एक संघर्ष मान कर जीने वाली अपने विचारों पर चाहे वह कितनी ही Rigid क्यों न हो, अंत तक अड़े रहने वाली लेकिन साहसी महिला है जो समाज और धर्म को दरकिनार कर अपने प्रेमी से विवाह कर लेती है, लेकिन प्रेमी-प्रेमिका को परस्पर विश्वास का अंकुर पति-पत्नी बन जाने पर एक ‘वटवृक्ष’ की तरह उन्नत कराने में असहाय सिद्ध होती है और यहीं पर नाटक का आशय और मूल स्वभाव विभु कुमार स्पष्ट करते हैं।
नाटक में बोली जाने वाली भाषा चाहे वह ठेठ छत्तीसगढ़ी हो या उपनगरीय (यहां मेरा आशय ‘हिंग्लिश’ अर्थात् इंगलिश मिश्रित हिन्दी से है), संवाद ‘बोल्ड’ और प्रभावी हैं। विभु कुमार के नाटकों का शक्तिस्थान प्रभाव व स्फूर्त संवाद हैं।
उदाहरण: ‘आजादी के इतने वर्षों बाद भी यह देश एक छत के नीचे नहीं आ पाया है। जानते हो मिस्त्री, क्यों ? क्योंकि पचास वर्ष बाद भी ये राजनेता देश की छत तक नहीं ढाल पाये हैं।’
‘मकान में जब दो प्यार भरे दिल रहते हैं तब वह घर बनता है। ‘या’ सपने में अचानक धर्म कहां आ गया ? क्या सपनों का भी अलग अलग धर्म होता है ? या सपने भी हिंदू या मुसलमान होते हैं ?’
अपने अनूठे दृष्टिकोण और आक्रामक विचारों के बावजूद विभु कुमार मंचन की दृष्टि से निर्देशक को मेहनत-मशक्कत करवाने में कसर नहीं छोड़ते। अपने तेज़-तर्रार संवादों और शाब्दिक मायाजाल बुनने में वे पूरे खरे उतरे हैं। लेकिन नाट्यमंचन करने में सहायक ‘प्रसंग निर्मित’ में निर्देशक की मानो परीक्षा ले ली है। पहले अंक की समाप्ति तक पता चल जाता है
कि नाटक अपनी यही निर्बाध गति बनाये रखेगा और निर्देशक को अपनी क्रियाशीलता (Creativity) उसी गति से लगातार बनाये रखनी होगी व प्रसंगों को यथोचित (Directorial Touch) देते रहना होगा, वरना किस क्षण नाटक अचानक मोड़ ले कर प्रचार-नाट्य (Propaganda-play) की ओर झुकता जाएगा, इस बात पर अंकुश लगाना कठिन कार्य हो जाएगा।
यह बात कहकर मैं विभु कुमार के इस नाटक पर प्रचार-नाट्य का आरोप क़तई नहीं लगा रहा हूं। क्योंकि प्रचार-नाट्य किसी ख़ास विषय का तात्कालिक मुद्दों पर अपनी बात बहुत ही बोझिलाना अंदाज में प्रेक्षकों पर उंडेलते रहते हैं जैसे, स्त्रियों का शोषण, अंधविश्वास, पानी की समस्या या पर्यावरण आदि। इन नाटकों में विचारों को प्राधान्य दिया जाता है, लेकिन नाट्यमयता नदारद हो जाती है। ऐसे नाटक तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक विषय ताज़े हों। समस्याओं का समाधान होने पर नाटक स्वत: ही काल की गोद में चले जाते हैं।
विभु कुमार ने इस नाटक में भी कुछ समस्याओं को छुआ है, लेकिन समस्याओं का समाधान खोजने में उन्होंने प्रचार-तंत्र का सड़ा-गला रूप त्याग कर नये समाज के प्रतिरूप नौजवान पीढ़ी को अपने ताज़े रूप में प्रस्तुत कर इस दिशा में अलग रास्ता चुना है।
इस नाटक का नौजवान Charity begins at home के सिद्धान्त के अनुरूप वैचारिक परिवर्तन लाने गली-मुहल्ले या समाज से नहीं, बल्कि सीधे अपने घर से शुरूआत करने का बीड़ा उठाता है। इसी Positive note पर नाटक की इतिश्री होती है।
नाट्य-निर्देशक,
महाराष्ट्र नाट्यमंडल
महाराष्ट्र नाट्यमंडल
- मोहन कुंटे
पात्र
पुरुष,युवक-योगेश
मिस्त्री, तांगे वाला, वेटर- रेज़ा
युवती, महिला, मां- परवीन
लड़का-1, लड़का-2
खान साहब, भाई, अशरफ़
[नेपथ्य से मकान बनाने संबंधित विभिन्न आवाज़े-मसलन रेती, सीमेंट, गिट्टी आदि मिलाने की आवाज़ें। तसला पटकने, करनी चलाने की आवाज़।]
मिस्त्री: लकर लकर हाथ-गोड़ ल चला न। मेहंदी लगे हे का तोर हाथ मां ? तुमन ला तो काम पे रखेच के धरम नइये।
रेज़ा: काम के बेरा मज़ाक झन करे कर मिस्त्री। मजाक के बेरा में मजाक ह बने लगथे।
मिस्त्री: तब फेर हाथ-गोड़ ला लकर लकर काबर नई चलावत हस ? काम करे बर आये हस ते अपन चेहरा ला दिखाये बर।
रेज़ा: दस हाथ-गोड़ कर लौं का ? फेर महिच अकेल्ला हवं का ? अऊ रेजा मन भी तो हवयं। ओमन ला काबर नई बोलस। ओमन तोला कुछ देथे का ?
मिस्त्री:जादा पटर पटर झन कर। मैं अब्बड़ हरामी मनखे आंव।
रेज़ा: तोला अब्बड़ जानथौं। का करबे ? ठेकेदार ला बोलके छुट्टी करा देबे, करा दो। काम के कमी नइये।
[पुरुष का प्रवेश]
पुरुष: ऐ राजा, अपना काम कर। दो बात बोल दिया तो क्या हो गया ?
इज़्ज़्त नहीं चली गयी। (चारों तरफ़ देखते हुए मिस्त्री से) कैसा चल रहा है, मिस्त्री ?
मिस्त्री: देखत हो हस, साहब ! दिमाग़ चांट जाथें ए रेजा मन।
रेज़ा: अटर-पटर बात झन कर, मिस्त्री।
पुरुष: तुम चुप नहीं रह सकतीं; बाई ?
रेज़ा: तैं नई जानथस, साब। ये मिस्त्री के सुभाव ह ऐसनेच हे। कोनो रेजा एला नई भावय।
मिस्त्री: (व्यंग्य से) मोला का बिहाव करे बर हे, जउन हं तुहंर नखरा ल, सहंव।
पुरुष:मिस्त्री, तुम भी बेकार में उलझते रहते हो।
रेज़ा: समझ गे न साब मोर बात ला। एकर इही सुभाव ले हमन चिडथन।
मिस्त्री: (चिढ़कर) चल अपन काम कर। पानी-बादर के दिन हे। पानी गिरगे त सब्बो बोहा जाही। नुसकान साहब के होही। तोला का ! तोला तो अपन मजूरी ले मतलब....मालिक के ऐसी-तैसी।
रेज़ा: सुनत हस साहब, एकर गोठ ला। अइसन गोठियाए जाथे, औरत जात संग।
पुरुष: ढंग से बात किया करो, मिस्त्री। तुम्हारी साथिन है आख़िर।
मिस्त्री: तैं नई जानस साब। अब्बड़ चालू होथें ये रेजा मन, अऊ कामचोर घलोक।
पुरुष: (झुंझला कर) मिस्त्री, ये रेजाएं तुम्हारे साथ काम करती हैं। इज़्ज़्त किया करो। अपमानित होने या गाली सुनने घर से बाहर नहीं निकली हैं। (पॉज़)
कामचोर कौन नहीं है, मिस्त्री ? मैं, तुम, इस देश के नेता, मंत्री, अफ़सर-कौन नहीं है कामचोर ? ये बेचारी तो मजबूरी में ऐसा करती हैं। ज़रा सुस्ताने के लिए। (तल्खी़ से) साले सब के सब कामचोर हैं। (सोच की मुद्रा) आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यह देश एक छत के नीचे नहीं आ पाया.....जानते हो मिस्त्री, क्यों ?
[इस बीच रेज़ा चली जाती है।]
मिस्त्री: नई सकौं सॉब।
पुरुष: (कड़वाहट भरे स्वर में) साले आज़ादी के बाद से देश की एकता की छत ढाल रहे हैं....पचास वर्ष हो गये.....आज तक नहीं ढाल पाये। (आवेश में आ जाता है) राजनीति के इन्हीं मिस्त्रियों की मिलीभगत है, कारस्तानी है, मिस्त्री। (नफ़रत से) ये साले चाहते हैं नहीं कि देश में एकता हो।
मिस्त्री: काबर ?
पुरुष: इसलिए मिस्त्री कि एकता होने से इनकी कुर्सी ख़तरे में पड़ जाएगी।
मिस्त्री: तैं हमर देस के छत के गोठ ला करत हस का ! (भोलेपन से) कइसन होथे साहब देस के छत ह ?....(ऊंची आवाज़ में) ए हरिया, देख के पानी मिलाबे। मसाला गिल्ला झन होवय। अइसन कर, थोरकुन सीमेंट अऊ मिला दे।
[इन संवादों के बीच मकान बनाने का अभिनय चलता रहेगा। निर्देशक अपने ढंग से इंप्रोवाइज़ कर सकता है।]
पुरुष: देश की छत एकता से बनती है, मिस्त्री ! ये हरामख़ोर नेता नहीं चाहते कि देश में एकता रहे, वरना इनकी दुकानदारी कैसे चलेगी ?
मिस्त्री: सियान के सियानी गोठ।
पुरुष: जनता की इसी उदासीनता के कारण तो ये नेता ऐश कर रहे हैं और आम जनता बदहाल है। मिस्त्री: तौं साहब उचहा सियानी के गोठ करथस।...(रेज़ाओं को ऊंची आवाज़ में) अरे मसाला ला, जल्दी जल्दी लानव। पानी गिर जही तऽऽ तुमन भर देहू का साहब के नुकसान ला।
[तसला ले कर उसी रेज़ा का प्रवेश]
रेज़ा: हमन जादा देर नई रुकन, मिस्त्री।
[पुरुष काम का मुआयना कर रहा है।]
मिस्त्री: काबर ?
रेज़ा: अब्बड़ दूर जाये पड़थे हमन ला।
मिस्त्री: (झुंझला कर) साहब ल बोल, अपने मकान ला तोरेच घर तीर बनवा लै।
पुरुष: तुम सीधी बात क्यों नहीं करते, मिस्त्री ?
पुरुष: लात के देवता बात क्यों नई मानय, साब।
पुरुष: काम ज़रा जल्दी निपटाने की कोशिश करो। इनका कहना भी ठीक है।
मिस्त्री: (समझाने का भाव) छत ढलाइ के काम कह ह, एकेच घांव में कर जाथे साब, कतको बेरा हो जाये, अऊ कतको बड़ छत होवै। (पॉज़)
साहब, छतेच हा तो सबोच कुछ छत बिगड़थे त सबो कुछ बिगड़थे। छतेच ले घर के सुंदरइ हे, अऊ सुरक्षा घलोक हे, साहब। (बुज़ुर्गाना अंदाज़) छत ह मेहरिया सहिन होथे साहब। छत ह कमसल होगे, त घर ह कंसल हो जाये।
पुरुष: मिस्त्री, बातें तुम बड़ी ज्ञान की करते हो।
मिस्त्री: छत ढारत-ढारत सीख गेओं, साहब। किसम किसम के छत ढारत आये हवौं, अऊ किसम किसम के मेहरिया घलौक देखे हंव। छत अऊ मेहरिया के मामला मा बेपरवाही नई बरते कर चाही। दूनो ह कभू गिर सकथे। गिरना दूनो के सुभाव हे, साब।
पुरुष: देश के साथ भी यही बात है, मिस्त्री ! एकतारूपी छत कमज़ोर होगी तो कोई देशवासी उसके नीचे नहीं आएगा। सब अपनी अपनी छत बनाएंगे- क्षेत्रीयता की, सांप्रदायिकता की, जातीयता की। नेता इसे ही भुनाते हैं। जनता को उल्लू बना कर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
मिस्त्री: किसन भगवान हा इही ख़ातिर गोबरधन परबत ला उठाये रहिस।
पुरुष: (हंसतेव हुए) हां, भई मिस्त्री। किसन महाराज की लीला अपरंपार है।
मिस्त्री: ये मकान ल बना के तैं खुस नई अस का, साब ?
पुरुष : तुम्हें ऐसा क्योंकर लगा, मिस्त्री ?
मिस्त्री, तांगे वाला, वेटर- रेज़ा
युवती, महिला, मां- परवीन
लड़का-1, लड़का-2
खान साहब, भाई, अशरफ़
[नेपथ्य से मकान बनाने संबंधित विभिन्न आवाज़े-मसलन रेती, सीमेंट, गिट्टी आदि मिलाने की आवाज़ें। तसला पटकने, करनी चलाने की आवाज़।]
मिस्त्री: लकर लकर हाथ-गोड़ ल चला न। मेहंदी लगे हे का तोर हाथ मां ? तुमन ला तो काम पे रखेच के धरम नइये।
रेज़ा: काम के बेरा मज़ाक झन करे कर मिस्त्री। मजाक के बेरा में मजाक ह बने लगथे।
मिस्त्री: तब फेर हाथ-गोड़ ला लकर लकर काबर नई चलावत हस ? काम करे बर आये हस ते अपन चेहरा ला दिखाये बर।
रेज़ा: दस हाथ-गोड़ कर लौं का ? फेर महिच अकेल्ला हवं का ? अऊ रेजा मन भी तो हवयं। ओमन ला काबर नई बोलस। ओमन तोला कुछ देथे का ?
मिस्त्री:जादा पटर पटर झन कर। मैं अब्बड़ हरामी मनखे आंव।
रेज़ा: तोला अब्बड़ जानथौं। का करबे ? ठेकेदार ला बोलके छुट्टी करा देबे, करा दो। काम के कमी नइये।
[पुरुष का प्रवेश]
पुरुष: ऐ राजा, अपना काम कर। दो बात बोल दिया तो क्या हो गया ?
इज़्ज़्त नहीं चली गयी। (चारों तरफ़ देखते हुए मिस्त्री से) कैसा चल रहा है, मिस्त्री ?
मिस्त्री: देखत हो हस, साहब ! दिमाग़ चांट जाथें ए रेजा मन।
रेज़ा: अटर-पटर बात झन कर, मिस्त्री।
पुरुष: तुम चुप नहीं रह सकतीं; बाई ?
रेज़ा: तैं नई जानथस, साब। ये मिस्त्री के सुभाव ह ऐसनेच हे। कोनो रेजा एला नई भावय।
मिस्त्री: (व्यंग्य से) मोला का बिहाव करे बर हे, जउन हं तुहंर नखरा ल, सहंव।
पुरुष:मिस्त्री, तुम भी बेकार में उलझते रहते हो।
रेज़ा: समझ गे न साब मोर बात ला। एकर इही सुभाव ले हमन चिडथन।
मिस्त्री: (चिढ़कर) चल अपन काम कर। पानी-बादर के दिन हे। पानी गिरगे त सब्बो बोहा जाही। नुसकान साहब के होही। तोला का ! तोला तो अपन मजूरी ले मतलब....मालिक के ऐसी-तैसी।
रेज़ा: सुनत हस साहब, एकर गोठ ला। अइसन गोठियाए जाथे, औरत जात संग।
पुरुष: ढंग से बात किया करो, मिस्त्री। तुम्हारी साथिन है आख़िर।
मिस्त्री: तैं नई जानस साब। अब्बड़ चालू होथें ये रेजा मन, अऊ कामचोर घलोक।
पुरुष: (झुंझला कर) मिस्त्री, ये रेजाएं तुम्हारे साथ काम करती हैं। इज़्ज़्त किया करो। अपमानित होने या गाली सुनने घर से बाहर नहीं निकली हैं। (पॉज़)
कामचोर कौन नहीं है, मिस्त्री ? मैं, तुम, इस देश के नेता, मंत्री, अफ़सर-कौन नहीं है कामचोर ? ये बेचारी तो मजबूरी में ऐसा करती हैं। ज़रा सुस्ताने के लिए। (तल्खी़ से) साले सब के सब कामचोर हैं। (सोच की मुद्रा) आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यह देश एक छत के नीचे नहीं आ पाया.....जानते हो मिस्त्री, क्यों ?
[इस बीच रेज़ा चली जाती है।]
मिस्त्री: नई सकौं सॉब।
पुरुष: (कड़वाहट भरे स्वर में) साले आज़ादी के बाद से देश की एकता की छत ढाल रहे हैं....पचास वर्ष हो गये.....आज तक नहीं ढाल पाये। (आवेश में आ जाता है) राजनीति के इन्हीं मिस्त्रियों की मिलीभगत है, कारस्तानी है, मिस्त्री। (नफ़रत से) ये साले चाहते हैं नहीं कि देश में एकता हो।
मिस्त्री: काबर ?
पुरुष: इसलिए मिस्त्री कि एकता होने से इनकी कुर्सी ख़तरे में पड़ जाएगी।
मिस्त्री: तैं हमर देस के छत के गोठ ला करत हस का ! (भोलेपन से) कइसन होथे साहब देस के छत ह ?....(ऊंची आवाज़ में) ए हरिया, देख के पानी मिलाबे। मसाला गिल्ला झन होवय। अइसन कर, थोरकुन सीमेंट अऊ मिला दे।
[इन संवादों के बीच मकान बनाने का अभिनय चलता रहेगा। निर्देशक अपने ढंग से इंप्रोवाइज़ कर सकता है।]
पुरुष: देश की छत एकता से बनती है, मिस्त्री ! ये हरामख़ोर नेता नहीं चाहते कि देश में एकता रहे, वरना इनकी दुकानदारी कैसे चलेगी ?
मिस्त्री: सियान के सियानी गोठ।
पुरुष: जनता की इसी उदासीनता के कारण तो ये नेता ऐश कर रहे हैं और आम जनता बदहाल है। मिस्त्री: तौं साहब उचहा सियानी के गोठ करथस।...(रेज़ाओं को ऊंची आवाज़ में) अरे मसाला ला, जल्दी जल्दी लानव। पानी गिर जही तऽऽ तुमन भर देहू का साहब के नुकसान ला।
[तसला ले कर उसी रेज़ा का प्रवेश]
रेज़ा: हमन जादा देर नई रुकन, मिस्त्री।
[पुरुष काम का मुआयना कर रहा है।]
मिस्त्री: काबर ?
रेज़ा: अब्बड़ दूर जाये पड़थे हमन ला।
मिस्त्री: (झुंझला कर) साहब ल बोल, अपने मकान ला तोरेच घर तीर बनवा लै।
पुरुष: तुम सीधी बात क्यों नहीं करते, मिस्त्री ?
पुरुष: लात के देवता बात क्यों नई मानय, साब।
पुरुष: काम ज़रा जल्दी निपटाने की कोशिश करो। इनका कहना भी ठीक है।
मिस्त्री: (समझाने का भाव) छत ढलाइ के काम कह ह, एकेच घांव में कर जाथे साब, कतको बेरा हो जाये, अऊ कतको बड़ छत होवै। (पॉज़)
साहब, छतेच हा तो सबोच कुछ छत बिगड़थे त सबो कुछ बिगड़थे। छतेच ले घर के सुंदरइ हे, अऊ सुरक्षा घलोक हे, साहब। (बुज़ुर्गाना अंदाज़) छत ह मेहरिया सहिन होथे साहब। छत ह कमसल होगे, त घर ह कंसल हो जाये।
पुरुष: मिस्त्री, बातें तुम बड़ी ज्ञान की करते हो।
मिस्त्री: छत ढारत-ढारत सीख गेओं, साहब। किसम किसम के छत ढारत आये हवौं, अऊ किसम किसम के मेहरिया घलौक देखे हंव। छत अऊ मेहरिया के मामला मा बेपरवाही नई बरते कर चाही। दूनो ह कभू गिर सकथे। गिरना दूनो के सुभाव हे, साब।
पुरुष: देश के साथ भी यही बात है, मिस्त्री ! एकतारूपी छत कमज़ोर होगी तो कोई देशवासी उसके नीचे नहीं आएगा। सब अपनी अपनी छत बनाएंगे- क्षेत्रीयता की, सांप्रदायिकता की, जातीयता की। नेता इसे ही भुनाते हैं। जनता को उल्लू बना कर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
मिस्त्री: किसन भगवान हा इही ख़ातिर गोबरधन परबत ला उठाये रहिस।
पुरुष: (हंसतेव हुए) हां, भई मिस्त्री। किसन महाराज की लीला अपरंपार है।
मिस्त्री: ये मकान ल बना के तैं खुस नई अस का, साब ?
पुरुष : तुम्हें ऐसा क्योंकर लगा, मिस्त्री ?
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book